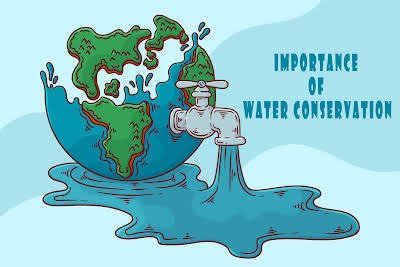लेखक: अंकित तिवारी प्रयागराज के स्वतंत्र पत्रकार और जल साक्षरता पे काम करते है
विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है इसका उद्देश्य विश्व के सभी देशों में स्वच्छ एवं सुरक्षित जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना और जल संरक्षण के महत्व पर भी सबका ध्यान आकर्षित करना है। इस वर्ष 2025 की थीम है “ग्लेशियर संरक्षण”, जिसके तहत जलवायु में बर्फ, हम और ग्लेशियरों के बीच संबंध और इसके महत्व पर जोर दिया गया है । संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार में भी यह स्पष्ट होता है कि सरकार को प्राणी मात्र के लिए पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। समय-समय पर न्यायपालिका के अनेक फैसले भी इस बात की पुष्टि करते हैं । जल का नाम संस्कृत में जीवन है मनुष्य द्वारा प्राकृतिक चीजों से छेड़छाड़ बढ़ती जा रही है । जनसंख्या , नदी विवाद, अत्यधिक जल दोहन शहरीकरण, औद्योगिक निर्माण, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, कृषि मेऔ जल संसाधनों का कुप्रबंधन आदि इसके प्रमुख कारणों में शामिल है।
आज विश्व में भयानक जल संकट का सामना करना पड़ रहा है । विभिन्न राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा जारी तमाम रिपोर्ट से इसकी पुष्टि होती है। इन सबकी जानकारी के बावजूद, हम जल संरक्षण को लेकर गंभीर नहीं हो रहे हैं ।
नीति आयोग के अनुसार भारत में केवल चार प्रतिशत जल संसाधन उपलब्ध है । देश के 21 प्रमुख शहर भीषण जल संकट की समस्या से जूझ रहे हैं। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2 करोड़ से अधिक बच्चे अत्यधिक जल संकट का सामना कर रहे हैं। जहां पर पानी की कमी है वहां पानी इकट्ठा करने में अधिकतम 25 मिनट का समय लगता है । घंटों बूंद बूंद पानी जमाकर काम चलाना पड़ता है।
विश्व बैंक ने बताया कि गर्मी आते ही पानी, भारत में सोने की तरह कीमती वस्तु बन जाता है । भारत में मुश्किल से 1/3 वर्षा के पानी का उपयोग कर पाता है ।वर्षा हमारे देश में मात्र चार-पांच महीने ही होती है जबकि पानी की जरूरत 12 महीने की होती है।
हिमालय पर बर्फबारी में रिकॉर्ड कमी से जल संकट की आशंका भयावह होती जा रही है। हमारी 12 प्रमुख नदी घाटियों से 23% जलापूर्ति होती है। हिमालय इस क्षेत्र में लोगों के लिए ताजे जल का महत्वपूर्ण स्रोत है । रिपोर्ट के अनुसार बर्फबारी में उतार-चढ़ाव से पानी की कमी देखने को मिल रही है । यूनेस्को की एक रिपोर्ट में 41.82% क्षेत्र सूखाग्रस्त है। समग्र जल प्रबंधन सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1994 में पानी की उपलब्धता प्रति व्यक्ति 6000 घन मीटर थी जो 2025 आते आते घटकर 1600 घन मीटर रह जाने का अनुमान है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्षा जल का मात्र 15% ही उपयोग में लाया जाता है शेष जल की मात्रा नदियों नालों से होता समुद्र में चला जाता है । यूनिसेफ के अनुसार स्वच्छ पेयजल 50% से कम भारतीयों को बड़ी मुश्किल से मिल पाता है । भारत सरकार के अनुसार आज पानी की उपलब्धता प्रति व्यक्ति वर्ष 1947 के मुकाबले केवल 18% है । वैज्ञानिकों के अनुसार जलवायु परिवर्तन की वजह से बेमौसम बरसात हो रही, सूखा पड़ रहा है । वर्ष 2100 आने तक हिमालय के 75 फीसदी ग्लेशियर पिघल जायेंगे , रिपोर्ट के अनुसार ग्लेशियर पिघलने के कारण गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु जैसी हिमालयी नदियों का प्रवाह कम हो जाएगा । ”ड्राफ्ट अर्ली वार्निंग ” सिस्टम के अनुसार देश का 41.52 फीसदी हिस्सा सूखा ग्रस्त है । यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले दो दशकों से वर्षा की मात्रा में गिरावट दर्ज की जा रही है इसलिए खेती किसानी के लिए भूमिगत जल का ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है । इससे भूजल दोहन लगातार बढ़ रहा है। जितना भी बारिश का पानी जमीन में अंदर जाता है उसका करीब 80 फीसदी सिंचाई और पीने के लिए निकल जाता है ।
वर्ष 2021-22 में कैग रिपोर्ट के एक रिपोर्ट के अनुसार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और काफी हद तक उत्तर प्रदेश में 100 फीसदी भूमिगत जल का दोहन हो रहा है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के करीब 25 शहर 2030 तक डे जीरो की कगार पर होंगे डे जीरो का मतलब पानी की आपूर्ति के लिए पूरी तरह अन्य साधनों पर आश्रित होना है । इसका एक कारण, उन क्षेत्रों के भूमिगत जल में फ्लोराइड की मात्रा काफी ज्यादा है। सरकार के एक सर्वे में देश के 25 राज्यों के 209 स्थानों पर भूमिगत जल में आर्सेनिक की मात्रा अधिक पाई गई है। यह हृदय और फेफड़ों के रोगों को बढ़ावा देता है । हालांकि यह बड़ी बात है सरकार के जल शक्ति मंत्री ने संसद को बताया कि आर्सेनिक प्रभावित बस्तियों की संख्या घटकर 314 रह गई अगस्त 2019 से फरवरी 2025 तक शेष बस्तियों में जल शोधन संयंत्र के माध्यम से स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया गया है। ग्लोबल कमिशन ऑन द इकोनॉमिक्स ऑफ़ द वाटर की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस दशक के अंत तक दुनिया भर में ताजे पानी की आपूर्ति की मांग 40 फीसदी तक बढ़ जाएगी। पानी की कमी और बढ़ती गर्मी से खाद्यान्न आपूर्ति भी 16 प्रतिशत घट जाएगी।
प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि नदी उत्सव की परंपरा को विस्तार दिया जाए इसे वर्तमान पीढ़ी को पानी का महत्व समझ में आएगा। सरकार जल संकट से निपटने के लिए कई तरह की नीतियां बना रही है जल शक्ति मंत्रालय स्थापित किया गया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जल शक्ति अभियान, कैश द रेन अभियान, अटल भूजल योजना, गंगा मिशन व जल निकायों की मरम्मत, जल वन और पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा, जल जीवन मिशन योजना विश्व की सबसे बड़ी योजना है । मोदी जी ने मन की बात में जल संकट से निपटने के लिए जनभागीदारी की अपील की है । हमें इसको गंभीरता से लेना होगा हम अपनी रोज के दैनिक जीवन में कुछ आदतें अपना कर, जल संकट से निपटने में अपना योगदान दे सकते हैं यदि किसी नल से एक सेकंड में एक बूंद पानी गिर रहा है तो 1 साल में 11000 लीटर से ज्यादा पानी बर्बाद होगा। भारत में 33% लोग रोज ब्रश करने के दौरान नल खुला रखते हैं जिससे 50 मिनट में 30 लीटर पानी बहता है। एक आर ओ वाटरफिल्टर वेस्ट से भी 45 लीटर पानी रोज बरबाद होता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार एक प्यूरीफायर 1 लीटर पानी शुद्ध करने में 3 लीटर पानी वेस्ट होता है यानी आपके घर में रोज 15 लीटर पानी शुद्ध करने में 45 लीटर पानी वेस्ट भी होता है ।
प्लास्टिक छोड़ने से भी पानी की बचत होगी। एक किलोग्राम प्लास्टिक बनाने में 180 लीटर पानी लगता है। समय पर गार्डनिंग करने से साल में पानी के लिए सुबह सूरज चढ़ने के पहले और शाम सूरज ढलने के बाद का समय होता है क्योंकि तब पानी सीधे जमीन के नीचे जाने की संभावना रहती है । गार्डन में सही समय पर पानी देकर 100 लीटर पानी बचाया जा सकता है । एक रोटी की बर्बादी यानि 35 लीटर पानी की बर्बादी, दुनिया में पानी की खपत का 92% हमारी खेती में जाता है। यूएनओ के रिपोर्ट के अनुसार हर साल हर व्यक्ति करीब 74 किलोग्राम भोजन बर्बाद करता है रिपोर्ट के अनुसार 1 किलोग्राम गेहूं पैदा करने के लिए 1000 लीटर पानी लगता है। इससे अंदाजा लगा लीजिये कि कितने करोड़ लीटर पानी हम बर्बाद करते हैं। रासायनिक खेती भी तीनगुना अधिक पानी खर्च करती है। पारंपरिक खेती मात्र एकतिहाई जल से संभव है। हम भारतीयों को वर्षा जल संरक्षण पर ध्यान देने की जरूरत है । खासकर शहरों में वर्षाजल संरक्षण अनिवार्य है यदि हर घर, इमारत, सोसायटी, बिल्डिंग वर्षा जल संरक्षण करे तो सबसे पहले उसे खुद हर पांचवें साल बोरिंग गहरा नहीं करवाना होगा, सालों भर निर्बाध जल मिलेगा और भूजल स्तर बढ़ेगा जिसकी घोर जरूरत है। यह ज्यादा खर्चीला भी नहीं है। हर बिल्डर या मालिक पानी के लिए बोरिंग करवाने के साथ रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग भी अपनाए तो स्थितियां बेहतर होने लगेगी।